आज देर शाम को रायपुर से फोन के मार्फत सूचना मिली कि आज की 'नई दुनिया' के रविवारीय पन्ने पर मेरा एक अनुवाद छपा हुआ है ; निज़ार क़ब्बानी की एक छोटी - सी कविता का अनुवाद। अब यह अख़बार हमारी तरफ़ मिलता नहीं । पता नहीं कब देखने को मिले। अच्छा लगा कि एक कविता प्रेमी की हैसियत से जो कुछ अनुवाद कार्य मैं चुपचाप कर रहा हूँ वह पत्र - पत्रिकाओं के माध्यम से धीरे - धीरे कविता प्रेमियों - पाठकों तक पहुँच पा रहा है। लीजिए , इसी क्रम में आज एक बार फिर सीरियाई कवि निज़ार क़ब्बानी ( 21 मार्च 1923 - 30 अप्रेल 1998) की एक और कविता का यह अनुवाद...
निज़ार क़ब्बानी की कविता
वर्षा उत्सव
(अनुवाद : सिद्धेश्वर सिंह)
किसी एक ठाँव ठिकाना नहीं मेरा
अप्रत्याशित है मेरा हाल मुकाम
एक पागल मछली की मानिन्द दूर तलक की है मेरी यात्रा
मेरे रक्त में ज्वाल है
चिंगारियाँ हैं मेरी आँखों में।
अन्वेषण कर रहा हूँ समीरण की स्वतंत्रता का
वश में कर लिया है अपने भीतर के घुमंतुओं को
दौड़ रहा हूँ हरिताभ मेघों के पीछे
अपनी आँखों से पी रहा हूँ हजारों छवियों को
अग्रसर हूँ यात्रा के अंतिम पड़ाव तक की यात्रा पर।
जलयात्रा पर हूँ एक दूसरे अंतरिक्ष की ओर
उठ रहा हूँ गर्द - गुबार से
भूल रहा हूँ अपना नाम
भूल रहा हूँ वनस्पतियों की संज्ञा
वृक्षों का इतिहास
उड़ान भर रहा हूँ सूर्य से
वहाँ की ऊब थकाने लगी है अब
भाग रहा हूँ नगरों- बस्तियों से
शताब्दियाँ बीत गईं सोया नहीं
चंद्रमा के पदतल में।
अपने पीछे छोड़ रहा हूँ
कँचीली आँखे
पथरीला आकाश
अपना पैतृक वास - स्थान
मुझे सूर्य की ओर लौट चलने के लिए न कहो
क्योंकि अब मैं सम्बद्ध हूँ बारिश के उत्सव संग।
--
(* चित्र : एलेना रोमानोवा की पेंटिंग - रेड अम्ब्रेला)







.jpg)


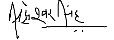.jpg)